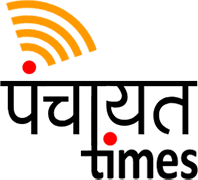फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ एक ऐसे शायर जिन्हें अंग्रेजी, उर्दू, फ़ारसी और अरबी ज़बान में महारथ हासिल थी. उन्होंने हिंदी, उर्दू, फ़ारसी और पंजाबी में रचनाएं लिखी. फ़ैज़ की पैदाइश 13 फरवरी, 1911 को भारत के सियालकोट (अब पाकिस्तान) में हुई. विभाजन के बाद फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ भी उन्ही लोगों में से थे जो नए मुल्क में चले गए. उन्हें विभाजन का बहुत दुःख था और यह दुःख उनकी एक नज़्म में साफ़ देखा जा सकता है, जिसमे वह लिखते हैं-
“ये दाग़-दाग़ उजाला ये शब ग़ज़ीदा शहर, वो इंतज़ार था जिसका ये वो शहर तो नहीं”
इश्क़-मोहब्बत से आगे
यूं तो अमूमन शायरों को इश्क़, मोहब्बत और महबूब के सिवाय कुछ नज़र नहीं आता. वो सिर्फ़ महबूबा की ज़ुल्फ़ों में ही इलझ के रह जातें हैं. लेकिन फ़ैज़ इन सब से ऊपर उठकर लिखते थे. शुरुआत में ज़रूर उनकी भी शायरी में ‘प्यार-मोहब्बत’ देखा जा सकता है, लेकिन जब उन्होंने आम लोगों के दर्द को लिखना शुरू किया तो फिर वह ऐसा था कि उनके लिखे कलाम किसी मज़लूम को हिम्मत देने के लिए काफ़ी है. फ़ैज़ साहब इस ‘प्यार-मोहब्बत’ से निकालकर लोगों का दर्द टटोल रहे थे, तो उन्होंने लिखा-
“मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग”
फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ सेना में भी रहे और उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध में भी शिरकत की. उन्होंने ज़िन्दगी की हर धूप और छांव को बड़े क़रीब से देखा. उन्होंने कई आंदोलनों, दुःख-दर्द और यातनाओं को महसूस कर अपने कलम में उतारा. यही वजह थी कि उन्होंने इश्किया शायरी से निकलकर लोगों के दर्द को लिखा. वो लिख्त्ते हैं-
“लौट आती है उधर को भी नज़र क्या कीजे, अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजे, और भी दुःख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा”
यानी फ़ैज़ साहब मानते हैं कि अब भी उनका महबूब उतना ही ख़ूबसूरत है, लेकिन उससे भी बड़ा और ज़रूरी फ़र्ज़ शायर के लिए यह है कि वह कमज़ोर और मज़लूमों की आवाज़ बने.
ख़ामोश मिजाज़ी फ़ैज़

फ़ैज़ साहब की ज़िंदगी दुखों और यातनाओं का एक लंबा सफ़र है. वह तबियत से बहुत ही नर्म और खामोश मिजाज़ी थे. उनकी बेटी मुनीज़ा हाशमी अपने वालिद के बारे में बताती हैं कि वह बहुत ही ख़ामोश तबियत के थे. दादी जब तक उन्हें दूध पीने के लिए नहीं बोलती थीं, तब तक वह ख़ुद नहीं मांगते थे.
लेकिन ख़ामोश तबियत होने के बावजूद भी फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ ने ज़ुल्म के ख़िलाफ़ चुप्पी नहीं साधी. हमेशा हक़ के लिए आवाज़ उठाई. वह क्रांति के शायर थे और लोगों को जगाने वाले थे. उन्होंने पाकिस्तानी हुकूमत के ख़िलाफ़ भी खुलेआम बगावत की. जिसके लिए वह जेल भी गए. जेल के दिनों को वह काग़ज़ पर उतारते हुए लिखते हैं-
“आशिक़ी की तरह जेलखाना भी एक बुनियादी तजुर्बा है, जिसमे फ़िक्र-ओ-नज़र का आधा दरीचा ख़ुद खुल जाता है, बाहरी जगत की दूरी और वक़्त ज़ाया हो जाते हैं, पास की चीज़ भी दूर हो जाती है, और दूर की चीज़ भी बहुत क़रीब”
फ़ैज़ सिर्फ़ अपने मुल्क के लोगों की ही आवाज़ नहीं बने, बल्कि उन्होंने फ़िलिस्तीन, अफ़्रीका और ईरानी लोगों के दर्द को भी उठाया. मतलब फ़ैज़ को इंटरनेशनल शायर कहें तो इसमें ताज्जुब नहीं होना चाहिए. ज़ुल्म और मज़लूमों के लिए जलने वाली यह लौ लाहौर में 20 नवंबर 1984 को हमेशा के लिए बुझ गई.