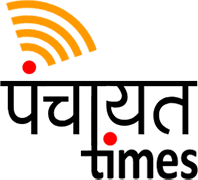नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य विधानसभाओं ने पारित विधेयकों को मंजूरी देने, वापस करने या राष्ट्रपति को भेजने के लिए राज्यपालों के लिए समयसीमा निर्दिष्ट करते हुए पाकिस्तान और अमेरिका के संविधानों का संदर्भ दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि समय-सीमा का उल्लंघन न्यायिक जांच के लिए उत्तरदायी है क्योंकि इसने राष्ट्रपति को विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए तीन महीने की समय-सीमा निर्धारित की है।
अनुच्छेद 75 का हवाला दिया
8 अप्रैल को दिए गए और शुक्रवार को ऑनलाइन जारी किए गए अपने 415-पृष्ठ के फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 75 का हवाला दिया, जिसके अनुसार देश के राष्ट्रपति को 10 दिनों के भीतर किसी विधेयक पर निर्णय लेना चाहिए। यदि उस अवधि के भीतर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, तो विधेयक को मंजूरी मिल गई मानी जाती है।
फैसले को लिखते हुए न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला ने लिखा उदाहरण के लिए, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के संविधान का अनुच्छेद 75 या अमेरिकी संविधान का अनुच्छेद I, खंड 7, जहां यदि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई निर्णय नहीं लिया जाता है, तो विधेयक को मंजूरी मिल गई मानी जाती है।
पाकिस्तान और अमेरिका के संविधानों का संदर्भ दिया
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने, वापस करने या राष्ट्रपति को भेजने के लिए राज्यपालों के लिए समयसीमा निर्दिष्ट करते हुए पाकिस्तान और अमेरिका के संविधानों का संदर्भ दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि समय-सीमा का उल्लंघन न्यायिक जांच के लिए उत्तरदायी है क्योंकि इसने राष्ट्रपति को विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए तीन महीने की समय-सीमा निर्धारित की है।
पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति को 10 दिनों के भीतर विधेयक को मजलिस-ए-शूरा (संसद) को या तो स्वीकृति देनी होती है या वापस करना होता है। यदि विधेयक वापस लौटा दिया जाता है और बाद में फिर से पारित किया जाता है, चाहे संशोधित हो या नहीं, राष्ट्रपति को अगले 10 दिनों के भीतर स्वीकृति प्रदान करनी होती है। ऐसा न करने पर, विधेयक को स्वचालित रूप से राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो जाती है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ऐसा प्रावधान कार्यकारी निष्क्रियता के विरुद्ध सुरक्षा के रूप में कार्य करता है और विधायी दक्षता को बढ़ावा देता है।
लेकिन न्यायालय ने कहा कि उसे पता है किदुनिया भर के कई देशों के विपरीत, जहां निर्दिष्ट समय अवधि की समाप्ति पर स्वीकृती प्रदान करने का प्रावधान किया गया है, हमारे संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।
शीर्ष न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि भारत के संवैधानिक ढांचे में इस तरह की लंबी निष्क्रियता अलोकतांत्रिक और अस्वीकार्य है।
राष्ट्रपति के पास भेजने का उनका निर्णय अवैध
इस प्रकार तमिलनाडु के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तिशाली शक्तियों का सहारा लेना पड़ा, ताकि यह निर्णय दिया जा सके कि विधानसभा द्वारा पारित किए गए लंबे समय से लंबित 10 विधेयक जिन पर राज्यपाल ने महीनों तक टालमटोल की थी, को उनकी स्वीकृति मिल गई है और घोषित किया कि विधानसभा द्वारा उन्हें पुनः पारित किए जाने के पश्चात उन्हें राष्ट्रपति के पास भेजने का उनका निर्णय अवैध है।
इसने कहा कि राष्ट्रपति ने ऐसे संदर्भित विधेयकों पर कोई भी निर्णय भी अमान्य होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समय सीमा के बिना, राज्यपाल लोकतंत्र के लिए खेल बिगाड़ सकते हैं। जहां निर्वाचित सरकार को नीतियों तथा चुनावी वादों को लागू करने के लिए पांच वर्ष का समय मिलता है।
न्यायालय ने कहा कि अनुचित और लंबे समय तक विधेयकों पर कोई कार्रवाई न करना वस्तुत राज्यपाल को पॉकेट वीटो की शक्ति प्रदान करता है और इसे हमारी संवैधानिक योजना के अंतर्गत अनुमेय नहीं माना जा सकता है।
पीठ ने यह भी याद दिलाया कि संविधान सभा की बहसों के दौरान डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने राज्यपालों को विधेयकों पर कार्रवाई करने के लिए छह सप्ताह की समय सीमा प्रस्तावित की थी। बाद में सरकारिया और पुंछी आयोगों ने भी इसी भावना को दोहराया तथा विधायी जवाबदेही की भावना को बनाए रखने के लिए समयबद्ध निर्णय लेने की वकालत की।